
भारत-चीन संबंध निबंध: Essay on India China
भारत-चीन संबंध हिंदी में निबंध
India-China relations: New rose on the grave of history full essay in hindi / भारत-चीन संबंध पर आधारित पूरा हिंदी निबंध 2019
Contents
शंका और संभावनाओं से आच्छादित क्षितिज
भारत के वैदेशिक संबंधों में सर्वाधिक शंकास्पद और रहस्यमय किंतु संभावनाशील और दूरगामी प्रभावक है तो भारत-चीन संबंध। इसको लेकर अलग-अलग अटकलें हैं और अलग-अलग आकलन किसी के अनुसार यह चीन के साथ अपने संबंधों का समर्पण करते हुए नेहरू के पंचशील सिद्धांतों के बखान की पुनरावृत्ति है तो किसी के अनुसार एक-ध्रुवीय अमरीकी वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए रूस-चीन-भारत द्वारा एक दूसरा महाशक्ति केंद्र बनाने की प्रक्रिया कोई इस शताब्दी को एशियाई शताब्दी बनाने का प्रयास कहता है तो कोई इतिहास के सैन्य संघर्ष के बोझ को हटाकर की जानेवाली भारत-चीन की नई आर्थिक जुगलबंदी। बहरहाल दोनों देशों के बीच सीमा-विवादों के चलते 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के अंतर्गत हुए 10 समझौते और साझे घोषणा-पत्र को न केवल भारत और चीन की 2.36 अरब जनता कुल विश्व की 40% जनता ने शका और औत्सुक्य से देखा है बल्कि अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान सहित शेष विश्व ने भी कौतुक भरी दृष्टि से निहारा है। इसके बाद मनमोहन सिंह की दो सरकारों ने भी उसी दिशा में चीन के साथ के संबंधों को व्यापारिक प्रगाढ़ता की ओर ही उन्मुख किया है।
कटु इतिहास के दर्द का एहसास
चीन का तिब्बत पर 1949 में हमला और फिर पंचशील सिद्धांतों तथा ‘ हिंद-चीन भाई-भाई’ के नारों के उद्घोष के बावजूद 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण अब तक भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बड़े हिस्सों पर चीन का दावा जताना, सिक्किम के भारत में विलय की अस्वीकृति पाकिस्तान को विकसित नाभिकीय प्रौद्योगिकी तथा अन्य सैनिक सहायता देना। आतंकवादी संगठनों को सैन्य सहायता की सुविधाएँ जुटाना तथा भारत और चीन के सौहार्दपूर्ण संबंधों के मार्ग में वे विशाल हिमालयी ग्लेसियर हैं जिन्हें दोनों देशों के राजनीतिक विवेक की उद्दाम ऊष्मा ही पिघला सकती है किंतु क्या इतिहास की समझ यह नहीं कहती है कि दूध का जला छाछ फुक-फुककर पीता रहेगा तो फिर क्या वह हमेशा के लिए दूध से वंचित नहीं हो जाएगा।
यह भी पढ़े: कश्मीर समस्या पर निबंध
भारत-चीन संबंध: समान सामर्थ्य और चुनौतियां
भारत और चीन वर्तमान वैश्विक मंदी के दौर में भी लगभग 6% (भारत) से 9% (चीन) तक की दर से अर्थव्यवस्थाओं को विकसित कर सकने में सक्षम रहे हैं। विश्व को एक-तिहाई जनसंख्या वाले और 30 साल से कम आयु के 55% की विरा युवा-शक्ति वाले ये दोनों देश विश्व के बहुत विशाल उपभोक्ता क्षेत्र तो हैं ही मानव संसाधन की प्रबल शक्ति के हैं। दोनों देशों की अधिकतम आबादी कृषि-समृद्धि से जुड़ी हुई है तथा दोनों ही अमेरिका और यूरोप की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के शोषण-चक्र से बचने के लिए बेचैन हैं। दो ही देश श्रम-बहुलता को अधुनातन तकनीकी सामर्थ्य से संपन्न कर अर्थव्यवस्था के नए मॉडल प्रारूप विकसित करना चाहते हैं और भारत एवं चीन की दोनों ही प्राचीन संस्कृतियाँ विश्व की अन्य संस्कृतियों से भिन्न परंपरा और विकास के द्वंद्व को अपने-अपने ढंग से खेल रही हैं।
नई संभावनाओं की तलाश
भारत चीन से संरचनात्मक ढांचे के विकास, पूंजीनिवेश की तकनीक, कंप्यूटर हार्डवेआर उत्पादन तथा उत्पादन प्रक्रिया में किफ़ायत की प्रक्रिया को सीख सकता है तो चीन भारत से निजी उद्यमशीलता, कॉरपोरेट गवर्नेस, पूंजी बाजार की क्षमता, सॉफ्टवेअर दवा एवं रसायन उत्पादन आदि की तकनीक को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों के साझा बाजार की तरह भारत और चीन भी साझा बाजार बन सकते हैं तथा विश्व के 40% थे पड़ोसी उपभोक्ता इस प्रक्रिया से सीधे लाभान्वित हो सकते हैं। दोनों देशों के हित अनेक दृष्टियों से समान हैं इसलिए कानकुन सम्मेलन (सितंबर, 2003) की तरह विश्व व्यापार संगठन में विकासशील एवं अविकसित देशों को समन्वित और संगठित नेतृत्व देकर विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के शोषण से बच सकते हैं। वस्तुतचीन से स्पर्धा करने की बेमानी बहस के बजाय दोनों देशों की विशाल अर्थव्यवस्थाओं के आदान-प्रदान एवं अनुपूरकता की संभावनाओं को तलाशने की ज़रूरत है। दोनों देशों के बीच पर्यटन सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा बौद्ध-दर्शन की वे समान स्वर-लहरियाँ तो हैं ही जिनमें दोनों ही आनंदित होकर अपने पुराने इतिहास-दर्द को ग़म-ग़लत कर सकते हैं।
भारत में आतंकवाद हिंदी में निबंध
भारत-चीन संबंध: बढ़ते संबंधों में नया मोड़
वाजपेयी की चीन यात्रा से 2002-03 में व्यापार (आयात-निर्यात) 4.2 अरब डॉलर पहुँच गया। सितंबर2003 में भारतीय प्रधानमंत्री की चीन-यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ के बीच सीमा रास्तों से व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ आपसी संबंधों को व्यापक बनाने वाला एक साझा घोषणा-पत्र भी जारी किया जिसमें सर्वोच्च शक्तिशाली देश अमरीका के कारण विश्व व्यवस्था पैदा हुए असंतुलन का पुनर्मूल्यांकन करना, आपसी सहयोग एवं संभावनाओं के साथ-साथ विश्वा शांति में ‘आसियान सिक्योरिटी फोरम’ में सहभागिता करना, संयुक्त नए संदर्भों राष्ट्र संघ की में उपजी भूमिका के मद्देनज़र काम करने की संभावनाएँ तलाशना, व्यापार संगठन ने तर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व तकनीकी विषमताओं समाप्त करना, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के ही साथ भारत-चीन कार्यदल द्वारा सीमा -रेखा पर संतुलन बनाने के प्रयास करना, चीन-पाक के हथियार व्यापार पर विचार करना, सीमा विवाद को हल करने का यथासंभव प्रयास करना, तिब्बत व सिक्किम संदर्भ में व्यावहारिक व उचित कार्यवाही करना तथा विपक्षीय व्यापार के साथ आर्थिक व सहयोग पर विशेष बल देना प्रमुख रहा है। इसके बाद मनमोहन सिंह की चीन यात्रा तथा चीनी प्रधानमंत्रियों की यात्राओं से उक्त संबंधो में प्रगाढता आई है, विषेस रूप से दोनों देशो के बीच आर्थिक संबंधो में व्यापकता आई है।
सीमा-विवाद नहीं, व्यापार को प्राथमिकता
भारत-चीन संबंधों के सीमा-विवाद को कोने में टाँगकर फिलहाल आर्थिक संबंधों की जतन बिछाने की कोशिश की गई है। चीन ने भारत में संरचनागत विकास हेतु 50 करोड़ डॉलर के निवेश की इच्छा व्यक्त की थी, सिक्किम के पास नाथूला दर्रा से व्यापार करने तथा तिब्बत के रेगिनगौंग में भारतीय व्यापार चौकी स्थापित करने की स्वीकृति दी, व्यापारिक वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई। चीन ने भारत से लौह-अयस्क, तंबाकू, जैव प्रौद्योगिकी के और अधिक आयात की संभावनाएँ जताई। 2008 में चीन में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों के समय तक चीन भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेअर को निर्यात करने तथा भारत से इस संबंध में सॉफ्टवेअर को आयात करने में पहल की। इस प्रकार भारत-चीन के बीच 2002-03 में 4.2 अरब डॉलर का हुआ व्यापार पिछले एक दशक कई गुना बढ़ गया। वस्तुतः अब दोनों देशों की व्यापारिक भुजा परस्पर जुड़ने को उठी हैं। यह व्यापार सँकड़े नाथूला दर्रा से बढ़कर व्यापक समुद्री मार्ग तक सघन हो गया है।
यह भी पढ़े: भारत में धर्मनिरपेक्षता हिंदी में निबंध
भारत-चीन संबंध: उपसंहार
उदारीकरण के दौर में अमरीकी-यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के नव-आर्थिक से साम्राज्यवाद बचाव करने, अमरीका की एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को नियंत्रित करने तथा भारत-चीन की 250 अरब जनसंख्या के आर्थिक-सांस्कृतिक हित में भारत-चीन के संबंधों में व्यापारिक दरें से ही सही नए राजनीतिक संबंधों के राजमार्ग की तलाश नए भविष्य की ऐतिहासिक आवश्यकता थी किंतु चीन से आशंका की नहीं सतर्कता की ज़रूरत है। 1962 की ठोकर के बाद उपजी 2012 तक की भारतीय सामरिक समृधि की यात्रा को चीन भी समझता है, उदारीकरण ने साम्यवादी चीन को व्यापारी चीन में बदला है, अतः इन बदली हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों दोनों को तैयार करने के लक्ष्यों को देखते हए पारंपरिक सैद्धांतिक रूढ़ता की बजाय कटु इतिहास की कब्र पर ‘पंचशील’ के साथ-साथ ‘अर्थशील’ के नये गुलाब उगाने चाहिए।

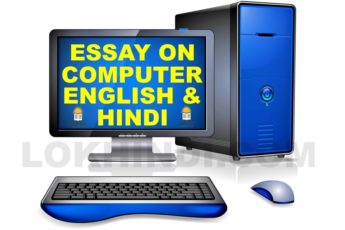
Leave a Comment